Class 12 Political Science Chapter 4 Notes in Hindi
सत्ता के वैकल्पिक केंद्र notes
यहाँ हम कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के पहले अध्याय “सत्ता के वैकल्पिक केंद्र” के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। इस अध्याय में सत्ता के नए केन्द्र से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।
ये नोट्स उन छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरल और व्यवस्थित भाषा में तैयार की गई यह सामग्री अध्याय को तेजी से दोहराने और मुख्य बिंदुओं को याद रखने में मदद करेगी।
Class 12 Political Science Chapter 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र notes
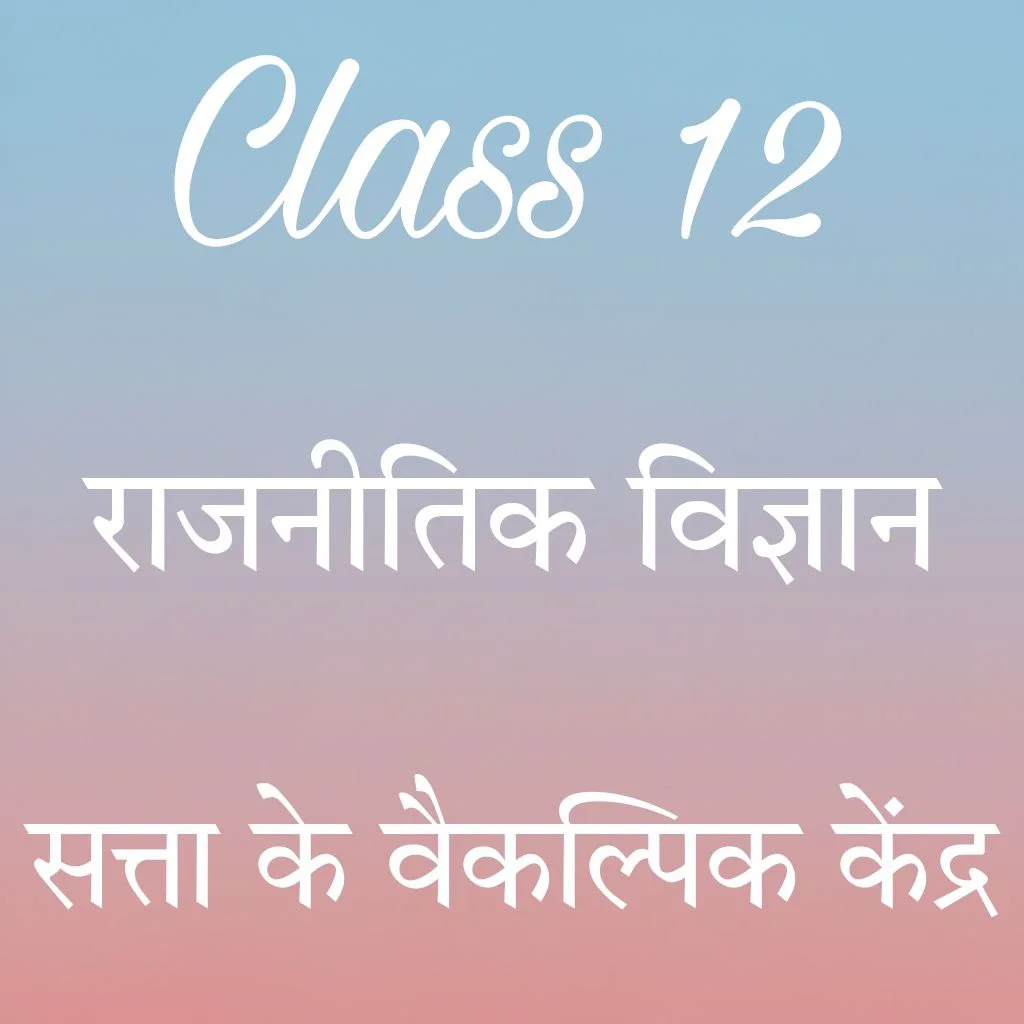
class 12 Political Science chapter 4 notes in hindi
सत्ता के नए केन्द्र का अर्थ:-
शीतयुद्ध के पश्चात अंतराष्ट्रीय राजनीति में कुछ संगठन और देशों ने अपनी एक प्रभावशाली भूमिका निभाई जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि यह संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि राजनैतिक और आर्थिक सत्ता के समकालीन केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे।
यूरोपीय संघ
यूरोपीय संघ का गठन
- 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो गया।
- युद्ध के पश्चात पूरे यूरोप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई।
- 1948 में अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत यूरोप के देशों को आर्थिक मदद देना शुरू किया।
- 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई।
- 1957 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया।
- 1979 में यूरोपीय संसद का गठन किया गया। जिसके बाद से यह संगठन आर्थिक संगठन से एक राजनैतिक संगठन के रूप में बदलना शुरू हो गया था।
- 1992 में मास्ट्रिस संधि द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ।
- 1992 में यूरोपीय संघ पूर्णरूप से एक राजनैतिक संगठन बन चुका था।
यूरोपीय संघ की स्थापना के कारण और उद्देश्य
- यूरोपीय संघ की स्थापना सदस्य देशों की एक समान नीति बनाने के लिए की गई थी।
- सभी सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ाने एवं सभी देशों में एक सामान मुद्रा(यूरो) का चलन हो सके ताकि अमेरिकी डॉलर की माँग को कम किया जा सके।
- संगठन के सदस्य देशों के बीच विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करके क्षेत्र में शान्ति की स्थापना की जाए।
- सभी सदस्यों के बीच सहयोग को बढाकर राजनैतिक,सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में तेजी से विकास करना है।
- संगठन के सदस्य देशों में मुक्त आवागमन को बढ़ा कर व्यापारिक कार्यों में तेजी करना।
- यूरोप के देशों को एक जगह संगठित करके और संगठन बनाकर अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को टक्कर देना था।
यूरोपीय संघ की विशेषताएं (अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर)
- यूरोपीय संघ के देशों ने अपने संगठन के लिए अपना झण्डा ओर्गान का का निर्माण किया जोकि इसको एक राजनैतिक संगठन दर्शाता है।
इसका अपना झंडा, गान,स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है। - यूरोपीय संगठन के सभी देशों की GDP को एक जगह संगठित करने पर वह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है जो कि अमेरिका को सीधी टक्कर दे सकता है।
- यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो की भागेदारी ने विश्व व्यापार में अमेरिकी डॉलर की मांग को 3 गुणा कम कर दिया है।
- यूरोपीय संघ की सैन्य शक्ति विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है।
- यूरोपीय संघ के दो देश ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु संपन्न देश होने के साथ-साथ सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्य भी है।
- संघ के सदस्यों में एक साझी विदेश नीति काम करती है जो कि संघ की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत स्थिति में पहुंचाती है।
- समय के साथ-साथ यूरोपीय संघ ने वैश्विक मंच पर अपने आर्थिक भूमिका के स्थान पर अपनी राजनैतिक भागेदारी को ज्यादा बढाया है।
- यूरोपीय संघ ने अमेरिकी एक ध्रुवीयता को सीधी टक्कर दी है जिसके कारण संघ एक नए वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है।
यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभावः
- 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17000 अरब डालर से ज्यादा था जो अमरीका के ही लगभग है।
- इसकी मुद्रा यूरो, अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है।
- विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से तीन गुना ज्यादा है।
- इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है।
- यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है।
यूरोपीय संघ के राजनैतिक प्रभावः-
- इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है।
- यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं।
यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभावः-
- यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है।
- इसका कुल रक्षा बजट अमरीका के बाद सबसे अधिक है।
- यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं।
- अंतरिक विज्ञान और संचार प्रोद्यौगिकी के मामले भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है।
यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ या सीमाएँ:-
1.) इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है जो कई बार एक-दूसरे के खिलाफ भी होती हैं। जैसे-इराक पर हमले के मामले में।
2.) यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है।
3.) डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिस्स संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया।
4.) यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमरीकी गठबंधन में थे।
5.) ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा।
6.) ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 मे एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया। जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है।
आसियान (ASEAN) Association of South Earth
- आसियाने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है।
- आसियान की स्थापना 1967 में बैंको घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 5 देशों ने मिलकर की- इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाइलैंड, मलेशिया, फिलीपींस।
- इन पांच देशों को आसियान का संस्थापक देश माना जाता है।
- इस संगठन में 5 देशों ने बाद में सदस्यता ली- वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई।
वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य शामिल है।
आसियान के गठन के कारण
- सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना ताकि वहाँ की जनता को सभी बुनियादी सुविधाएं मिल सके।
- संगठन के सदस्य देशों के बीच विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से हल करना।
- आसियान देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र का विस्तार करके व्यापारिक गतिविधियों को तेज करना
- सभी राष्ट्रों की सम्प्रभुता और सार्वभौमिकता बनाए रखना ताकि सभी देश अपने विचार और अपनी विदेश नीति को अपने निर्णयों के आधार पर कर सके।
- दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में शान्ति की स्थापना करना और व्यापारिक कार्यों को प्रोत्साहन देना।
आसियान का महत्व
- क्षेत्रीय स्तर पर आपसी मेलमिलाप को बढावा देना
- सदस्य देशों की सैन्य शक्ति का प्रयोग करना
- संगठन के सभी सदस्यो के बीच विदेश नीति का तालमेल बनाए रखना।
अधिक से अधिक मुक्त व्यापार क्षेत्र का विस्तार करके व्यापारिक गतिविधियों को तेज करना। - आर्थिक समुदाय, सामाजिक समुदाय और सुरक्षा समुदाय का गठन करके आसियान की नीतियों का विस्तार करना ताकि सभी सदस्य देशों को विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंचाया जा सके।
- विजन 2020 द्वारा आसियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करके सस्ता के नए विकल्प के रूप मे रखना।
आसियान शैली
सभी सदस्यों के साथ अनौपचारिक टकरात रहित और सहयोगात्मक मेलमिलाप को बढ़ावा देना ही आसियान शैली कहलाता है।
चीन
- 1949 में चीन को आजादी मिली उस समय चीन में कम्यूनिष्ट पार्टी का बोलबाला था।
- चीन में अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण में रखा गया था।
- 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। शुरूआत में यहाँ अर्थव्यवस्था सोवियत प्रणाली पर आधारित थी।
माओ के नेतृत्व में चीन का विकास :-
चीन ने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूँजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था।
1) चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया।
2) चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी।
3) कृषि परम्परागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी।
चीनी अर्थव्यवस्या का उत्थानः-
चीन में सुधारों की पहल :-
- चीन ने 1972 में अमरीका से संबंध बनाकर अपने राजनैतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया।
- 1973 में प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के चार प्रस्ताव रखे।
- 1978 में चीन में खुले द्वार की नीति (open door policy) अपनाया और वैश्वीकरण को महत्व देते हुए अपने देश में निवेशकों को काम करने का मौका दिया।
- 1982 में चीन ने कृषि क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिया।
- 1998 में औद्योगिक क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिया। जिसके कारण बाजार को महत्व दिया जाने लगा।
- अपने देश में विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए चीन ने पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ – Special Economic Zone) का गठन किया जहां से सारी की सारी व्यापारिक गतिविधियों को किया जाने लगा।
- पूरे विश्व में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (EDI) चीन में सबसे अधिक है और साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार (अमेरिकी डॉलर) भी विश्व में सबसे अधिक चीन के पास है।
- चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में तीसरे स्थान पर है और इसकी मुद्रा का नाम युयान है।
- चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल हो गया जिसका सीधा संकेत यह था कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के लिए खोल दी है।
- वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के आधार पर अमेरिका को सीधी टक्कर देने वाला चीन एक महाशक्ति के रूप में दिखाई देने लगा है।
चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू :-
(1) वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ।
(2) चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं।
(3) वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं है।
(4)गाँव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा है।
(5) विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफी हानि पहुँचाई है।
(6) चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा है।
चीनः विश्व की नई उमरती शक्ति के रूप में :
(1) क्षेत्रफल के हिसाब से विशाल आकार
(2) 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना
(3) विश्व की यह एक बड़ी अर्थव्यवस्था है
(4) जापान, अमरीका, आसियान और रूस- सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं।
(5) 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफी मदद की है।
(6) चीन परमाणु शक्ति संपन्न देश है।
(7)चीन सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य भी है।
(8) चीन द्वारा लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश तथा सहायता की इसकी नीतियां दर्शाती है कि चीन विश्व में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है।
चीन के साथ भारत के संबधः
विवाद के क्षेत्रः
1. 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर चीन द्वारा बस्तियों बनाने से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए।
2. अरूणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावे के चलते 1962 में भारत-चीन युद्ध हुआ।
3. 1962 के युद्ध में भारत की सैनिक पराजय हुई और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालीक असर हुआ।
4. 1976 तक दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध समाप्त ही रहे।
5. दोनों देशों के बीच हाल के समय हुए सीमा-विवाद से भी संबंधों में गिरावट आई है।
6. पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन मददगार है।
7. बांग्लादेश, म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को दक्षिण एशिया में भारत के हितों के खिलाफ माना जाता है।
8 संयुक्त राष्ट्रसंघ भारत के आतंकवादी प्रस्ताव के विरु) चीन वीटो शक्ति का प्रयोग कर पाकिस्तान को समर्थन देता है।
9. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन और भारत के संबंधों में गिरावट लाता है।
सहयोग के क्षेत्रः-
1. 1970 के दशके के उत्तर्राद्ध में चीन के राजनैतिक नेतृत्व बदलने से चीन की नीति में अब परिवर्तन हुआ। चीन ने वैचारिक मुद्दों के स्थान पर व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख किए इसलिए चीन भारत के साथ विवादास्पद मामलों को छोड़ संबंध सुधारने को तैयार हो गया।
2. दोनों देशों के संबंधों का राजनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है।
3. दोनों देश एशिया की राजनीति में और अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं।
4. दिसम्बर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा कर संबंधों को सुधारने का प्रयास किया।
5.दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर पोस्ट खोलने के समझौते किए।
6.1999 से भारत-चीन व्यापार लगभग 30 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रहा है।
7.1992 में भारत-चीन के बीच 33 करोड़ 80 लाख डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ।
8. 2017 में बढ़कर यह 84 अरब डालर का हो गया।
9. विदेश में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामले में भी दोनों देश सहयोग के लिए तैयार है।
10. परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित के कारण संबंध सकारात्मक हो रहे है।
11. चीन और भारत के नेता और अधिकारी अब अक्सर दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं।
जापान
- एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश
- परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है।
- जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं।
जापान सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में
- जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह ज्यादातर कच्चे माल का आयात करता है इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेजी हो प्रगति की।
- जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन(OECD) का सदस्य बन गया।
- 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह (G-7) के देशों में शामिल है।
- आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वा है।
परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है। - जापान संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट में 10% का योगदान करता है
- संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है।
- सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का सातवां स्थान है।
- 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है।
दक्षिण कोरिया
- कोरियाई प्राप्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया (रिपब्लिक ऑफ कोरिया) तथा उत्तरी कोरिया (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया) में विभाजित किया गया था।
- 1950-53 के दौरान ‘कोरियाई युद्ध’ और शीतयुद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया।
- अंत 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केन्द्र के रूप में उभरा।
दक्षिण कोरिया सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में :-
1. 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया का आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ जिसे “हान नदी पर चमत्कार” कहा जाता है।
2. 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना।
3. 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
4. सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में दक्षिण कोरिया का दसवां स्थान है।
5. मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18वां है।
6. दक्षिण कोरिया के उच्चमानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि शामिल हैं।
7. दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। सैमसंग, एलजी, हुंडई भारत में प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई ब्रांड है।
8.भारतीय और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते उनके बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते है।
ncert Class 12 Political Science Chapter 4 Notes in Hindi
के notes आपको कैसे लगे अपनी राय जरूर दे