एक दल के प्रभुत्व का दौर
Class 12 Political Science Chapter 2 Notes in Hindi
यहाँ हम कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के 2nd अध्याय “एक दल के प्रभुत्व का दौर” के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। इस अध्याय में एक दल के प्रभुत्व का दौर से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।
ये नोट्स उन छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरल और व्यवस्थित भाषा में तैयार की गई यह सामग्री अध्याय को तेजी से दोहराने और मुख्य बिंदुओं को याद रखने में मदद करेगी।
Class 12 political science Chapter 2 Notes in Hindi , एक दल के प्रभुत्व का दौर notes
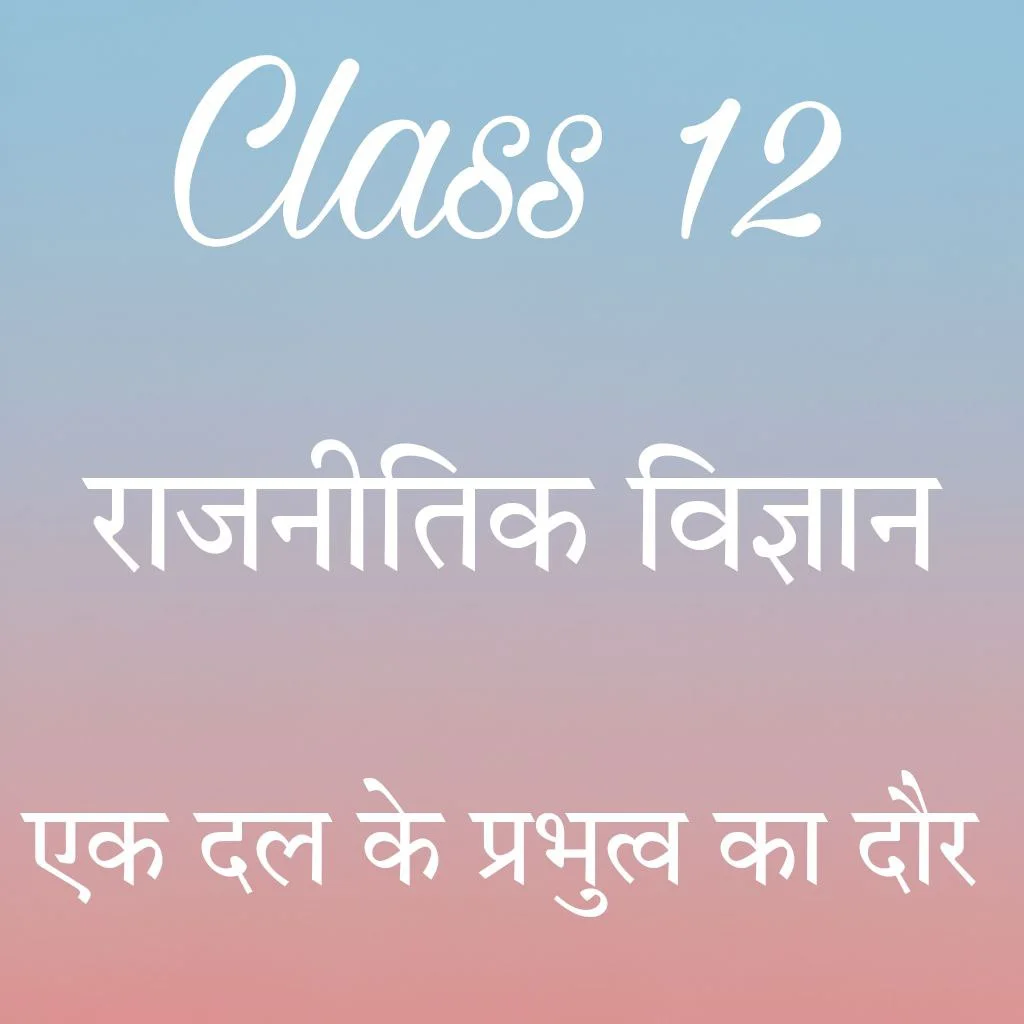
class 12 Political Science book 2 chapter 2 notes in hindi
एक दल के प्रभुत्व का दौर
- 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय देश में अंतरिम सरकार थी।
- अब संविधान के अनुसार नयी सरकार के लिए चुनाव करवाने थे।
- जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया।
- सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने।
- उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला चुनाव 1950 में हो जाएगी।
- भारतीय नेताओं की स्वतन्त्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में गहरी प्रतिबद्धता (आस्था) थी।
- इसलिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग और संसदीय प्रणाली का मार्ग अपनाया जबकि लगभग उसी समय स्वतंत्र हुए कई देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई।
चुनाव आयोग की चुनौतियाँ
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना।
- देश का बड़ा आकार
- विशाल जनसंख्या (17 करोड़ मतदाता)
- चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन
- मतदाता सूचियाँ बनाना (पहले प्रारूप में 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए, इन महिलाओं को अलां की बेटी,फलां की बीवी के रूप में दर्ज किया गया)
- साक्षरता की कमी – महज 15 फीसदी साक्षर
- चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण देना – 3 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया।
- इन्हीं कारणों से दो बार चुनाव स्थगित करना पड़ा।
- अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए।
पहला आम चुनाव
लगभग 17 करोड़ मतदाताओं द्वारा 3200 विधायक और 489 सांसद चुने जाते थे।
पहले आम चुनाव के बारे में राय
- एक हिन्दुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया।
- ‘ऑर्गनाइजर’ नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक – मताधिकार असफल रहा।
- भारत में पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952, तक हुए लेकिन क्योंकि ज्यादातर जगहों पर चुनाव 1952 में हुए इसलिए पहले आम चुनाव को 1952 के चुनाव कहा गया।
चुनाव प्रक्रिया
- चुनाव अभियान और मत गणना – 6 महीने लगे।
- हर सीट के लिए चार उम्मीदवार (औसतन)।
1952 के चुनाव के परिणाम
1.भारत में लोकतंत्र सफल रहा।
2.लोगो ने बढ़-चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लिया।
3.चुनाव में उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ,हारने वाले उम्मीदवारों ने भी परिणाम को सही बताया।
4.भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया।
5.चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीट जीती और सबसे बड़ी ‘पार्टी बन कर उभरी।
6.दूसरी सबसे बरी पार्टी रही कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसने 16 सीटें जीती।
7.जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने।
कांग्रेस का प्रभुत्व
- पहले तीन आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा।
- भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से इस प्रकार भिन्न रहा।
- मैक्सिको में PRI की स्थापना 1929 में हुई, जिसने मैक्सिको में 60 वर्षों तक शासन किया। परन्तु इसका रूप तानाशाही का था।
- बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ।
- चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों में संविधान सिर्फ एक ही पार्टी को अनुमति देता है।
- म्यांमार, बेलारूस और इरीट्रिया जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से कायम हुआ।
- भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों के होते हुए रहा है।
कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण
प्रथम तीन आम चुनावों में कांग्रेस का (एक दल का) प्रभुत्व रहा :-
i.स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका
ii.सुसंगठित पार्टी
iii.सबसे पुराना राजनीतिक दल
iv.पार्टी का राष्ट्र व्यापी नेटवर्क
v.प्रसिद्ध नेता
vi..सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की प्रकृक्ति।
vii.भारत की चुनाव प्रणाली।
- कांग्रेस की प्रकृति एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन की है। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बाशिंदे (रहने वाले) और गाँव के निवासी, मज़दूर और मालिक एवं मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली।
- कांग्रेस ने अपने अंदर गरमपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यमार्गियों विचार धाराओं को समाहित किया।
- कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने विपक्षी दलों के सामने समस्या खड़ी की और कांग्रेस को असाधारण शक्ति दी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक-दल की भूमिका निभायी और विपक्ष की भी।
- इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस-प्रणाली कहा जाता है।
विपक्षी पार्टियों का उद्भव
- 1950 के दशक में विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला।
- विपक्षी दलों ने शासक दल (कांग्रेस) पर अंकुश रखा।
- लोकतांत्रिक राजनीति में विकल्प की संभावना को जीवित रखा।
- विपक्षी दलों की मौजूदगी ने शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाये रखा।
सोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी पार्टी)
- विचारधारा – लोकतांत्रिक समाजवाद
- 1934 में कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं की एक की एक टोली द्वारा गठन कांग्रेस को ज्यादा परिवर्तनकारी और समतावादी बनाना चाहते थे।
- 1948 में कांग्रेस से अलग सोशलिस्ट पार्टी बनी।
- कांग्रेस की आलोचना- वह पूँजीपतियों और जमींदारी का पक्ष ले रही है और मजदूरों – किसानों की उपेक्षा कर रही है।
- सोशलिस्ट पार्टी के टुकड़े:-
- i.किसान मजदूर प्रजा पार्टी
ii.प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
iii.संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी - प्रमुख नेता – जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेन्द्र देव, राममनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी।
- मौजूदा दलों पर छाप – समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (युनाटेड), जनता दल (सेक्युलर)।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
- विचारधारा – साम्यवादी
- 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे।
- 1941 के दिसंबर में कांग्रेस से अलग हुए।
- इनके पास दूसरी और कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत आजादी के समर्थक एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित काडर मौजूद थे।
- इनका विचार था – 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आजादी नहीं थी ।
- प्रथम आम चुनाव में 16 सीटे जीती और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी।
- प्रमुख नेता- ए.के. गोपालन, एस. ए. डांगे, ई. एम. एस. नम्बुदरीपा , पी. सी जोशी, अजय घोष और पी. सुंदरैया।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई
i.भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी विचारधारा)
ii.भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सोवियत विचारधारा)
स्वतंत्र पार्टी
- स्थापना – 1959 के अगस्त मे
- सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था मे कम से कम हस्तक्षेप पर जोर।
- यह पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के हितों को छान में रखकर किए जारहे कराधान के खिलाफ थी। थी।
- कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान के आधार पर सरकारी नीति के विरुद्ध थी।
- विदेश नीति – गुटनिरपेक्षता की नीति व सोवियत संघ से रिश्ते को गलत मानती थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से नजदीकी संबंध बनाने की वकालत की।
- राजे-महाराजे, जमीदार, उद्योगपति आकर्षित हुए पर सामाजिक आधार की कमी इसलिए मजबूत नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाई।
- प्रमुख नेता – सी. राजगोपालाचारी, के. एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू-मसानी।
भारतीय जनसंघ
- स्थापना – 1951
- संस्थापक अध्यक्ष – श्यामा प्रसाद मुखर्जी
- एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर।
- अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने की पक्षधर थी।
- भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही।
- धार्मिक और सांस्कृतिक अपलसंख्यों को रियायत देने का विरोध।
- 1952 के चुनाव में 3 सीटें, 1957 के चुनाव में 4 सीटे जीती।
- प्रमुख नेता – श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय, बलराज।
- भारतीय जनता पार्टी की जड़े इसी जनसंघ में है।
ncert Class 12 Political Science book 2 Chapter 2 Notes in Hindi
के notes आपको कैसे लगे अपनी राय जरूर दे