Class 12 History Chapter 3 Notes in Hindi
बंधुत्व, जाति तथा वर्ग notes
(Kinship, Caste and Class)
यहाँ हम कक्षा 12 इतिहास के पहले अध्याय “बंधुत्व, जाति तथा वर्ग” के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। इस अध्याय में बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का दौर से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।
ये नोट्स उन छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरल और व्यवस्थित भाषा में तैयार की गई यह सामग्री अध्याय को तेजी से दोहराने और मुख्य बिंदुओं को याद रखने में मदद करेगी।
Class 12 History Chapter 3 Notes in Hindi , बंधुत्व जाति तथा वर्ग notes
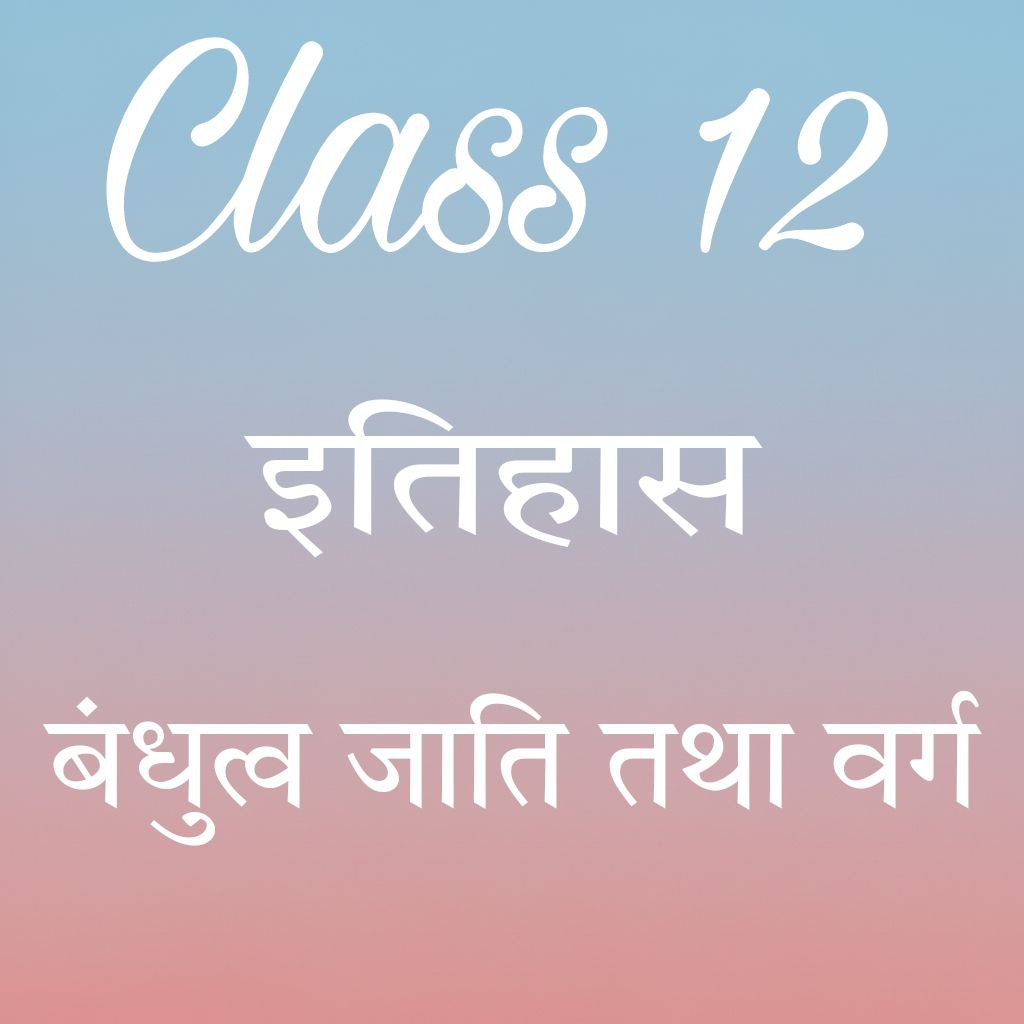
class 12 history chapter 3 notes in hindi
महाभारत
- महाभारत हिन्दू धर्म का एक महाकाव्य है।
- महाभारत के रचियता वेदव्यास को कहा जाता है।
- महाभारत में 18 पर्व है और 1948 अध्याय है।
- महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध का वर्णन है।
- महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी।
- महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला था।
श्रीमद्भागवत गीता
- कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही उपदेश श्रीमद्भागवत गीता में है।
- श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का सर्वाधिक इसमें निहित है।
- गीता में कुल 18 अध्याय एवं 700 श्लोक है।
- गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चालर्स विलयम्स ने किया।
महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन था?
महाभारत में आठ प्रकार के विवाह का वर्णन था।
- देव विवाह,
- आर्ष विवाह,
- प्रजापत्य विवाह,
- असुर विवाह,
- गन्धर्व विवाह,
- राक्षस विवाह और
- पिचाश विवाह।
इसमें प्रथम चार विवाह को उत्तम माना जाता था और अंतिम चार विवाह को निंदनीय माना जाता था।
महाभारत एक गतिशील ग्रंथ
- हिंदू परंपरा के अनुसार महाभारत के ग्रंथ के रचयिता महर्षि व्यास है उन्होंने इस ग्रंथ को श्री गणेश से परंतु बहुत से इतिहासकार इस विचार से सहमत नहीं है कि महाभारत ग्रंथ का एक ही रचयिता था।
- उनके विचार में यह एक गतिशील ग्रंथ है जिससे समय-समय पर बहुत कुछ जोड़ा गया ।
- कुछ अन्य लेखकों का कहना है “संभवतः मूल कथा के रचियता भारत सारथी थे जिन्हें ‘सूत कहां जाता था।
- यह क्षेत्रीय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजेता उपलब्धियों के बारे में कविता लिखते थे ।
महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण
1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी-एस- सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया।
(i) आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाय जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ़ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया।
(ii) इस परियोजना को पूरा करने में सैंतालीस वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आइ : पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई, वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए।
(iii) इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पादटिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्योरा देते हैं। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा।
(iv) कालांतर में विद्वानों ने पालि, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया।
इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किन्तु इन आदशो को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और कभीये-कभार इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा।
मनुस्मृति
- मनुस्मृति हिन्दू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र (स्मृति) है। इसे मानव-धर्म-शास्त्र, मनुसंहिता आदि नामों से भी जाना जाता है।
- धर्मग्रन्थकारों ने मनुस्मृति को एक सन्दर्भ के रूप में स्वीकारते हुए इसका अनुसरण किया है।
- मनुस्मृति का संकलन लगभग 200 ई-पू- से 200 ईसवी के बीच हुआ।
मनुस्मृति के अनुसार
पुरुषधन
- मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए किंतु जेष्ठ पुत्र विशेष भाँग का अधिकारी था।
- सामान्यतः भूमि पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था।मनुस्मृति के अनुसार पुरुष सात तरीके से धन अर्जित कर सकता है-
i.विरासत
ii.खोज,
iii.खरीद,
iv.विजित करके,
v.निवेश,
vi.कार्य द्वारा,
vii.सज्जनों द्वारा दी भेंट आदि।
स्त्रीधन
1.विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्रीधन अर्थात् स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी।
2. इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था।
मनुस्मृति के अनुसार 6 तरीके के संपत्ति अर्जित की हा सकती थी
(i) विवाह के मिली भेंट
(ii) स्नेह के प्रतीक के रूप में माता-पिता द्वारा उपहार
(iii) स्नेह के प्रतीक के रूप में भाई द्वारा प्राप्त उपहार
(iv) प्रवृत काल में प्राप्त उपहार
(v) अपने पति द्वारा प्राप्त उपहार
(vi) अपने पति द्वारा प्राप्त धन
महाभारत कालीन स्त्रियों की समस्याएं
(1) स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाता था।
(2) स्त्रियां पैतृक सम्पति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी।
(3) स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से निम्न थी।
(4) पत्नी को पति की संपति के रूप में माना जाता था।
(5) स्त्रियों को सीमित अधिकार ही प्राप्त थे।
पितृवंशिकता और मातृवंशिकता
पितृवंशिकता :
वह वंश परंपरा जो पिता, उसके बाद पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भमें सिंहासन पर भी अधिकार जमा सकते थे।
मातृवंशिकता :
वह वंश परम्परा जो माँ के नाम से जुड़ी होती है उसे मातृवंशिकता कहते है ।
बहिर्विवाह पद्धति
(i) जब किसी का विवाह अपने गोत्र से बाहर होता था तो विवाह पद्धति को बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता था ऐसा विवाह ब्राम्हणीय पद्धति के अनुकूल था ।
(ii) यह प्रथा इसलिए अपनाई जाती थी ताकि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था जिससे ‘उचित’ समय और ‘उचित’ व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात् विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया।
मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य
(i) शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था।
(ii) उच्च जाति के लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे वे इन चांडालो का स्पर्श, यहां तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे ।
(iii) मनुस्मृति में चांडालो के कर्तव्य की सूची मिलती है उन्हें गांव के बाहर रहना होता था । वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे।
(iv) चांडाल रात्रि में गांवों और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहिन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना पड़ता था ।
(v) अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बचाएं।
धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र
- नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हआ।
- यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद-फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान-प्रदान होता था।
- संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्नचिन्ह लगाए गए।
- इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताए तैयार कीं।
- ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था किन्तु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था।
- लगभग 500 ई-पू- से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया
वर्ण व्यवस्था
- भारत समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी।
- भारतीय समाज को चार वर्णों में बांटा गया था।
- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र।
- ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्ण का उत्पति विरत पुरुष के चार अंग से मानी गई है।
- ऐसा माना जाता है की ब्राह्मण के मुख से, क्षत्रिय बाहू से, वैश्य जंघा से और शुद्र पैर से उपन्न हुए हैं।
- ब्राह्मण का कार्य सम्पन्न करना, क्षत्रिय का काम रक्षा करना, वैश्य का काम व्यापार करना और शुद्र का काम इन तीनों वर्ण का सेवा करना था।
धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार चारों वर्णों के कार्य
(1) ब्राह्मण-अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना व करवाना, दान- दक्षिणा लेना।
(2) क्षत्रिय-युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढना, यज्ञ करवाना, दान-दक्षिणा देना।
(3) वैश्य- वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान-दक्षिणा देना, कृषि, गौ-पालन, व्यापार करना।
(4) शुद्र-तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना
क्या विवाह के समय गोत्र नियमों का पालन अनिवार्यतः होता था?
- नहीं।
- उदाहरण- सातवाहन राजाओं ने गोत्र प्रणाली के नियमों का पालन नहीं किया।
- सातवाहन राजाओं को उनके मातृ मातृनाम से जाना जाता था।
- सातवाहन राजाओं की रानियों ने विवाह के बाद भी अपने पिता के गोत्र को कायम रखते हुए अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण नहीं किया।
- सातवाहन राजाओं की कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी, यानि उनका अंतर्विवाह हुआ था।
गोत्र
- गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के साथ हसुसी ऋषि के वंशज माने जाते थे।
- गोत्र के प्रमुख दो नियमः-
- एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे।
- विवाह के पश्चात् स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना आता था ।
बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा
बहुपत्नी प्रथा
- एक पुरुष के अनेक पत्नी होने की परिपाटी बहुपत्नी प्रथा कहलाती है।
- जैसे:- पांडू की दो पत्नी थी कुंती एवं मोद्री
बहुपति प्रथा
- एक स्त्री के अनेक पति होने की परिपाटी बहुपति प्रथा कहलाती है।
- जैसे:- द्रौपदी एक पांच पति थे।
ncert Class 12 History Chapter 3 Notes in Hindi
के notes आपको कैसे लगे अपनी राय जरूर दे