पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन
Class 12 Political Science Chapter 8 Notes in Hindi
यहाँ हम कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के 8th अध्याय “पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन” के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। इस अध्याय में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।
ये नोट्स उन छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरल और व्यवस्थित भाषा में तैयार की गई यह सामग्री अध्याय को तेजी से दोहराने और मुख्य बिंदुओं को याद रखने में मदद करेगी।
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन Class 12 Political Science Chapter 8 Notes in Hindi
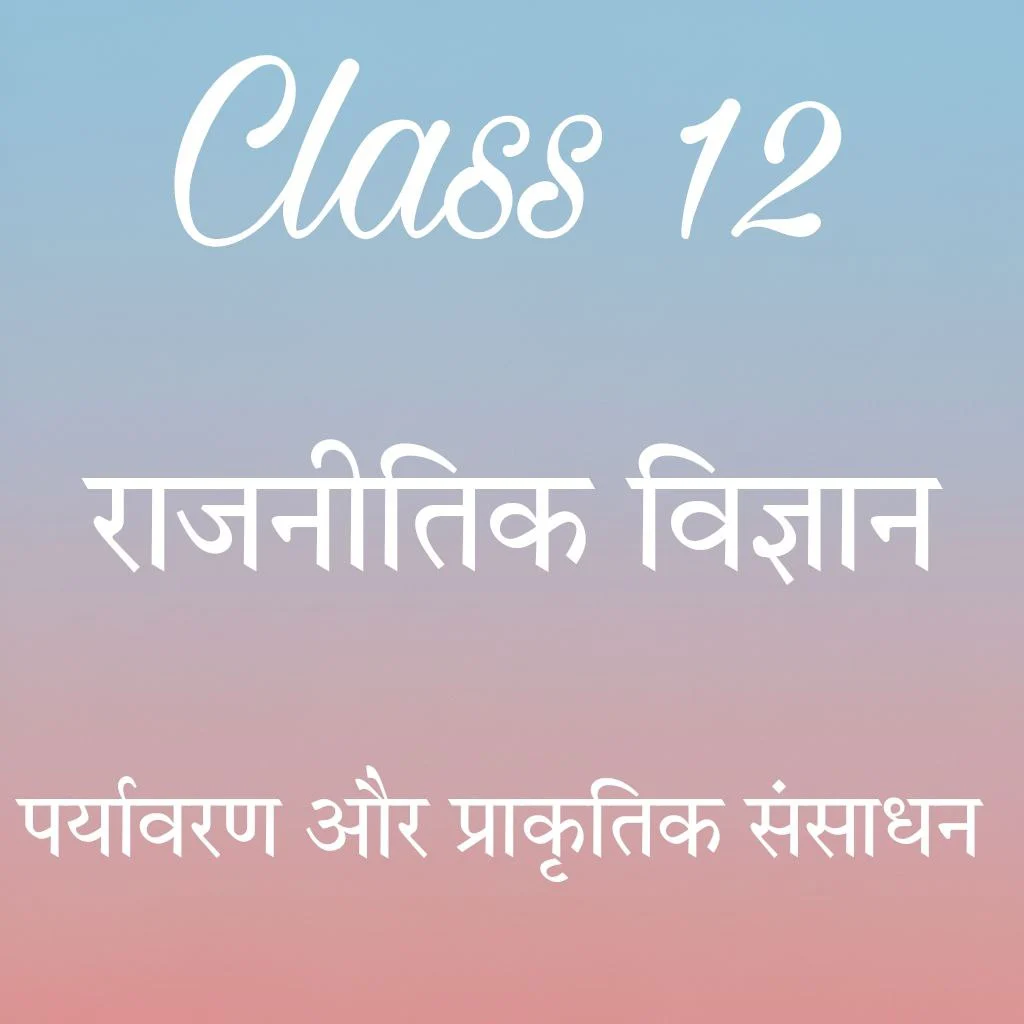
class 12 Political Science chapter 8 notes in hindi
पर्यावरण का अर्थ
परि (ऊपरी ) + आवरण इस का अर्थ है कि हमारे आस-पास के क्षेत्र मे आने वाली वनस्पति और जीव-जंतुओं को एक-साथ रखने वाले क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं।
प्राकृतिक संसाधन
प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं।
विश्व में पर्यावरण प्रदुषण के कारण
- जनसंख्या का तेजी से बढ़ना।
- वनों की कटाई से हरित क्षेत्र का कम होना।
- उपभोक्तावादी संस्कृति का तेजी से बढ़ना।
- प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
- औद्योगिकरण को बढ़ावा देना जिसके कारण पृथ्वी पर प्रदुषण में बढ़ोतरी होना।
- परिवहन के साधनों की अधिकता के कारण वायु प्रदुषण में तेजी से बढ़ोतरी होना।
- घरों में इस्तेमाल होने वाले AC और फ्रिज जैसे साधनों से क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उत्सर्जन होना।
रियो सम्मेलन (पृथ्वी सम्मेलन)
- 1992 में ब्राजील के रियो शहर में UNO द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया।
- इस सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया और साथ ही विश्व के अलग-अलग देशों से NGO और MNCs ने भी भाग लिया।
- इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी (वन) के आपसी संबंधों के लिए नियम बनाना था।
- इस सम्मेलन में सतत विकास को परिभाषित किया गया।
- इस सम्मेलन में एजेंडा -21 के रूप में विकास के लिए कुछ तरीके सुझाए गए।
साझी सम्पदा
साझी सम्पदा उन संसाधनों को कहते है जिन पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश का अधिकार न होकर पुरे समाज और पुरे विश्व का अधिकार होता होता है। जैसे- महासागर, ग्लैशियर, वायुमंडल, अंतरिक्ष, मैदान और नदियां इत्यादि साथ ही इसमें समुद्री सतह, आर्कटिक, अंटार्कटिक को भी शामिल किया गया है
साझी संपदा के लिए कुछ समझौते भी किया गए है:-
i.अंटार्कटिक संधि 1959
ii.मांट्रियल प्रोटोकोल 1981
iii. अंटार्कटिका प्रोटोकोल 1991
सांझी परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियां
- विकसित और विकासशील देशों के इस बारे में अलग-अलग मत है
- विकसित देश पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों मे बराबर बांटना चाहते है।
- जबकि विकासशील देशो का मानना है कि जो देश पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचाया है उस देश की जिम्मेदारी भी ज्यादा होनी चाहिए।
- साझी संपदा को इस्तेमाल करके विकसित देशों ने अपना खुद का आर्थिक विकास किया है जिसके कारण साझी संपदा को प्रदुषित करने में विकसित देशों की ज्यादा भूमिका है।
- विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में है इसीलिए वह अपने कार्यक्रमों को बीच में नहीं रोक सकते और पर्यावरण को बचाने के लिए जो दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे उनमें विकासशील देशों को छुट दी जानी आवश्यक है।
- उपरोक्त दिए गए कथनों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि विकसित देश विकास की चरम सीमा को प्राप्त कर चुके है इसी लिए उनको जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी पड़ेगी जबकि विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में ही है इसलिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
- साझी सम्पदा परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों यह भी दर्शाती है कि विश्व के सभी देशों को विकास करने का एकसमान अधिकार दिया जाए।
क्योटो प्रोटोकोल
- 1997 में जापान के क्योटो शहर में पर्यावरण समस्याओं को लेकर एक विश्व सम्मेलन हुआ इसी को क्योटो प्रोटोकोल कहा जाता है।
- इस सम्मेलन में United Nations framework convention on climate change पर हस्ताक्षर हुए जिसको क्योटो प्रोटोकोल कहा जाने लगा।
- भारत ने 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए।
- क्योटो प्रोटोकोल में भारत, चीन और बहुत से विकासशील देशी को प्रोटोकोल की बाध्यता से छुट दी गई।
- इसी सम्मेलन में यह माना गया कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण औद्योगिकीकरण है।
पर्यावरण आंदोलन
पर्यावरण सुरक्षा के लिए सक्रिय पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं और सरकारों द्वारा अंतरर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अनेक आंदोलन चलाए जाते है जिनका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना होता है
दक्षिणी देशों में मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका के देश और भारत में चलाए गए वन आंदोलन काफी महत्व रखते है।
ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरोध में आंदोलन चलाए गए
थाईलैंड, दक्षिण अफ्रिका, इंडोनेशिया, चीन और भारत में बड़े-बड़े बांधो का निर्माण किया गया तब-तब जनता ने सरकारों के खिलाफ पर्यावरण आंदोलन चलाए।
जलवायु परिवर्तन
- जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर सभी जीवित रूपों या सजीव वस्तुओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।
- जलवायु शब्द की सामान्य परिभाषा अपना अर्थ खो चुकी है क्योंकि मौसम कब बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता जिसका प्रभाव पर्यावरण पर दिखाई देता है जलवायु परिवर्तन के मुख कारणों में जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग, वनों की अत्यधिक कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन, परिवहन साधनों द्वारा वायु प्रदुषण और तेजी से बढ़ रहा औद्योगिकीकरण है।
- जलवायु परिवर्तन के परिणाम बहुत अधिक खतरनाक है जैसे वायुमंडल में तापवृद्धि, ओजोन परत में छिद्र होना, ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, कई क्षेत्रो मे अधिक वर्षा का होना और वनों मे लगने वाली आग शामिल है।
- जिस दर से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है यह काफी चिंताजनक है और यदि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आगे आने वाले 15-20 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान 1-5 डिग्री तक बढ़ सकता है।
- जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक रूप में पड़ रहा है जिसके कारण अचानक बारिश होने से या बहुत दिनों तक बारिश न होने सेे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। जिसके कारण खाद्यान्न की कमी हो सकती है।
- ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ने का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन ही है।
- जैसे-जैसे पृथ्वी में तापमान में बदलाव आ रहा है उसका सीधा असर ओजोन परत पर पड़ रहा है जिसके कारण ओजोन परत टूट गई है और सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही है।
- यदि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण में नहीं लाया गया तो पृथ्वी का अंत निकट है।
ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक ताप वृद्धि)
- वैश्विक ताप वृद्धि का सीधा सा अर्थ है कि पृथ्वी की सतह और वायुमंडल में औसत तापमान की दर धिरे धिरे बढ़ रही है
- वायुमंडल में Co₂ का स्तर बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को भी बढ़ा रहा है।
- यह सभी ग्रीन हाउस गैस कारक जलवाष्प, CO₂ , मिथेन, क्लोरो-फ्लोरोकार्बन, ओजोन आदि थर्मल विकरण को ज्यादा अवशोषित कर लेते है।
- वैश्विक कार्बन चक्र के कारण ओजोन परत में छिद्र बन चुका है जिसके कारण UV कितने पृथ्वी पर किरणे पृथ्वी पर पहुंच जाती है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है।
- ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण, जनसंख्या पर नियंत्रण और विनाशकारी प्रौद्योगिकी का कम उपयोग करके किया जा सकता है।
- विभिन्न देशों की सरकारें, निजी क्षेत्र और NGO द्वारा अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को धीरे-धीरे कम किया जा सके।
- अगर पृथ्वी को और उसके वायुमंडल को बचाना है तो सबसे महत्वपूर्ण काम यह होगा कि ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा।
- जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है उसका असर पृथ्वी पर साफ दिखाई देता है साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण वातावरण मे हो रहे बदलावों को भी हमें देखना होगा और इस दिशा में अहम कदम उठाने होंगे।
"लिमिट्स टू ग्रोथ " नामक पुस्तक
वैश्विक मामलो मे सरोकार रखने वाले विद्वानों के एक समूह ने जिसका नाम है-क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ ” लिखी। इस पुस्तक में बताया गया कि जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार संसाधन कम होते जा रहे है।
" अवर कॉमन फ्यूचर " नामक रिपोर्ट की चेतावनी
1987 में आई इस रिपोर्ट में जताया गया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके भविष्य में टिकाऊ साबित नही होंगे।
एजेंडा-21
इसमें यह कहा गया कि विकास का तरीका ऐसा हो जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।
एजेंडा -21 की आलोचना
इसमें कहा गया कि एजेंडा-21 में पर्यावरण पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
संसाधनों की भू-राजनीति
यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है। जिस देश के पास जितने संसाधन होगें उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी।
1) इमारती लकड़ी:- पश्चिम के देशों ने जलपोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो और विदेश व्यापार बढ़े।
2) तेल भण्डार:- विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास यूरेनियम और नेल जेस संसाधन थे। विकसित देशों ने नेल की निर्वाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गो पर सेना तैनात की।
3)जल :- पानी के नियन्त्रण एवं बँटवारे को लेकर लड़ाइयों हुई। जार्डन नदी के पानी के लिए चार राज्य दावेदार है इजराइल, जार्डन, सीरिया एवम् लेबनान ।
मूलवासी एवं उनके अधिकार
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में एसे लोगों को मूलवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया, भारत में ‘मूलवासी’ के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है 1975 में मूलवासियों का संगठन World Council of Indigeneous People बना।
- मूलवासियों की मुख्य माँग यह है कि इन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए, दूसरे आजादी के बाद से चली आ रही परियोजनाओं के कारण इनके विस्थापन एवं विकास की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संरक्षण का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण करना है।
- मूलवासियों के निवास वाले स्थान दक्षिण अमरीका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है जहां इन्हे आदिवासी या जनजाति कहा जाता है।
भारत का पर्यावरण सुरक्षा में योगदान
- 2002 क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर एवं उसका अनुमोदन।
- 2005 G-8 देशों की बैठक में विकसित देशों द्वारा की जा रही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पर जोर दिया।नेशनल ऑटो – फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग।
- 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया।
- 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया।
- भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है।
- भारत SAARC के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना।
- भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) की स्थापना की गई।
- भारत विश्व का पहला देश है जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय है।
- कार्बन गई ऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति कम योगदान
(अमेरिका 16 Ton, जापान 8 Ton, चीन 6 Ton, भारत 1.38 Ton) - भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए है।
- 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 73-75% कम करने का लक्ष्य रखा है।
- COP-23 में भारत वृक्षारोपण व वन क्षेत्र की वृद्धि के माध्यम से 2030 तक 2.5 से बिलियन टन Co₂ के बराबर सिंक बनाने का वादा किया है।
ncert Class 12 Political Science Chapter 8 Notes in Hindi
के notes आपको कैसे लगे अपनी राय जरूर दे