राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां
Class 12 Political Science Chapter 1 Notes in Hindi
यहाँ हम कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के पहले अध्याय “राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां” के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। इस अध्याय में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।
ये नोट्स उन छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरल और व्यवस्थित भाषा में तैयार की गई यह सामग्री अध्याय को तेजी से दोहराने और मुख्य बिंदुओं को याद रखने में मदद करेगी।
राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां Class 12 Political Science Chapter 1 Notes in Hindi
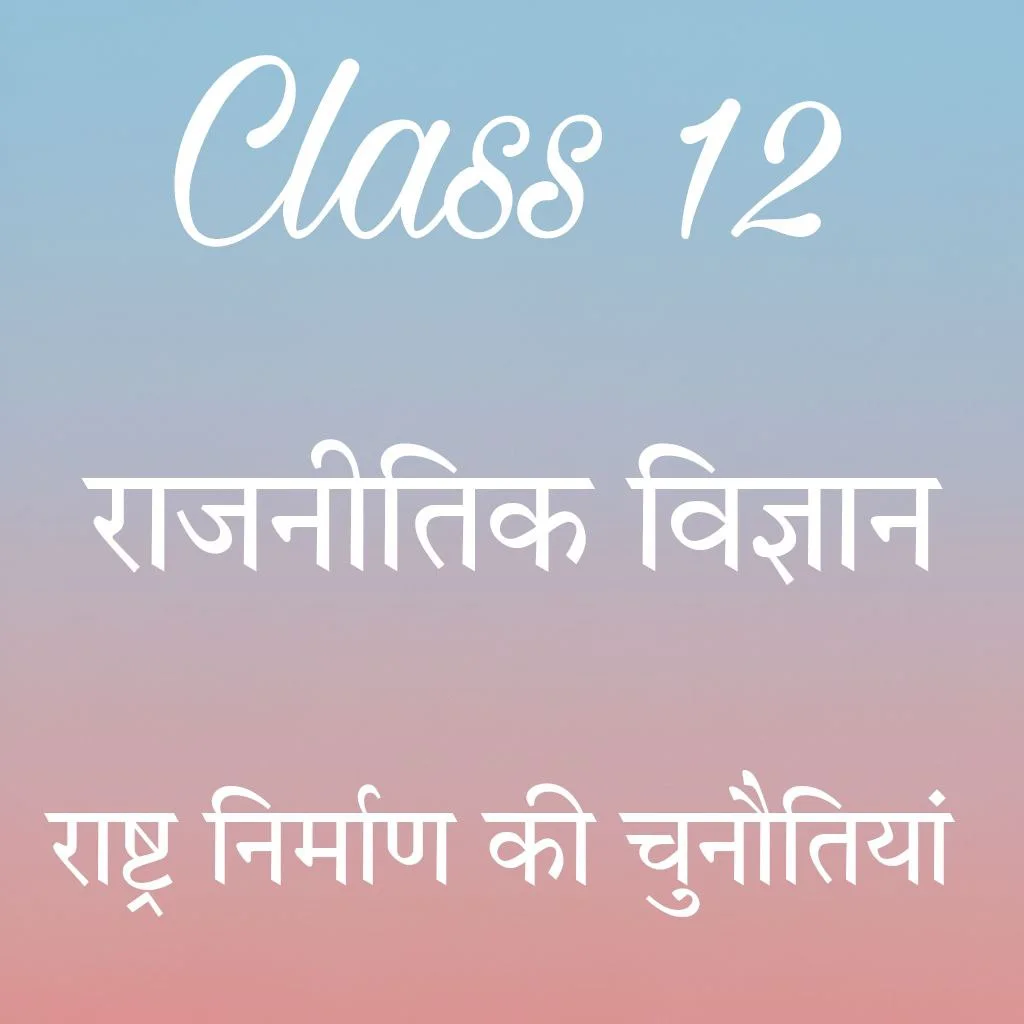
class 12 Political Science book 2 chapter 1 notes in hindi
राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां
- आजादी और द्वीराष्ट्र का सिद्धांत
- अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत को 1947 में आजादी मिली।
- कैबिनेट मिशन की सिफारिश थी कि भारत का विभाजन करके इसके दो टुकड़े कर दिए जाए एक पाकिस्तान दूसरा भारत।
- साथ ही रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वह अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती है या स्वतंत्र भीं रह सकती है बाद में वेवल योजना के तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान नाम का देश बनाया गया।
- 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दी इसी विभाजन को द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहा जाता है।
आजादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी।
i) आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जायेगा।
ii) सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी।
- 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग्य वधु से ‘चीर प्रतिष्ठित भेंट’ के द्वारा भारत के आजाद होने की घोषणा की।
आजाद भारत की चुनौतियां (1947 के बाद का भारत)
भारत को 1947 में आजाद होने के बाद तीन चुनौतियों का सामना करना पड़ा:-
1.एकता और अखंडता की चुनौती ( एकता के सुत्र में बांधना)
- सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण करना।
- विभिन्न भाषा, धर्म और संस्कृति के लोगों को मिलाकर एकता के सूत्र में बांधे रखना ताकि भारत की प्रभुसत्ता अखंड रहे।
- एक संपन्न भारत का निर्माण करना
- इस चुनौती को पुरा करने में सरदार वल्लभभाई पटेल की अहम् भूमिका रही।
2.लोकतंत्र की स्थापना करना
- लोगों को वोट डालने और चुनाव लडने कामधिकार देना।
- देश में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन संविधान के द्वारा करना।
- प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार देना।
- देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव समय पर कराना।
- देश के अंदर संविधान के अनुसार संसदीय और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की स्थापना करना।
3. समानता पर आधारित विकास
- समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सभी सुविधाएँ पहुंचाना
- भेदभाव को खत्म कर समानता का व्यवहार करना वंचित वर्गों, अल्पसंरक्षक वर्ग और अन्य पिछड़े समुदायों को विशेष सुविधाएँ देना
- विकास का प्रभाव सभी वर्गों पर एकसमान दिखाई देना।
- देश में विकास कार्यों के लिए कृषि क्षेत्र पर और उद्योग क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना
- विकास के लिए समाजवादी- उदारवादी मॉडल को अपनाना
- संविधान के द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय आयोग का गठन करना और देश में दीर्घकालीन विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ चलाना।
भारत का विभाजन
- मुस्लिम लीग ने ‘द्वि-राष्ट्र सिद्धांत’ को अपनाने के लिए तर्क दिया कि भारत किसी एक कौम का नहीं, अपितु ‘हिन्दू और मुसलमान’ नाम की दो कौमों का देश है और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की माँग की।
- भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया।
- जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हुई
(i)मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान।
(ii)मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के नेता खान-अब्दुल गफ्फार खाँ जिन्हें ‘सीमांत गांधी’ के नाम से जाना जाता है, वह ‘द्वि-राष्ट्र सिद्धांत’ के एकदम खिलाफ थे।
(iii)’ब्रिटिश इंडिया’ के मुस्लिम बहुल प्रान्त पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर-मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रान्तों का बँटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाकर किया गया।
(iv)भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था। इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे, कि उनका क्या होगा। वह कल से भारत के नागरिक होगें या पाकिस्तान के।
विभाजन की समस्या
- भारत-विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बँटने वाले इलाकों में हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़क उठे।
- पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर-बार, जमीन-जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भारत आना पड़ा और इसी प्रकार कुछ मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा।
- विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बँटवारा नहीं हुआ बल्कि भारत की सम्पदा का भी बँटवारा हुआ।
- आजादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली।
- लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यावहारिक रूप प्रदान किया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया।
विभाजन के परिणाम
- लोगों को अपनी घर और संपति को छोड़ना पड़ा।
- बड़ी संख्या में लोग हिंसा का शिकार हुए।
- अमृतसर और कोलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे हुए
- शरणार्थी लोगों के पुनर्वास की समस्या।
- महिलाओ और बच्चों के साथ बहुत अत्याचार हुए।
- औरतों के साथ जबरदस्ती शादी करना और धर्मपरिवर्तन कराना देखा गया।
- 80 लाख लोगो को घर छोड़ कर जाना पड़ा।
- 5-10 लाख लोगों की मौत हुई।
रजवाड़ो का विलय
- स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत दो भागों में बँटा हुआ था- ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतें।
- इन देशी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी।
- रियासतों के शासकों को मनाने-समझाने में सरदार पटेल (गृहमंत्री) ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ो को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया था।
- कैबिनेट मिशन ने यह शर्त रखी थी कि आप भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी भी देश में शामिल हो सकते हो और आप स्वतंत्र भी रह सकते हो।
- अधिकतर रजवाड़ो के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे।
- भारत सरकार कुछ इलाकों को थोड़ी स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी।
- विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखण्डता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था।
- अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये थे इस सहमति पत्र को ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ कहा जाता है।
- जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ।
- लेकिन बाद में इन चारों रियासतों को अलग-अलग तरीके से भारत में शामिल कर लिया गया।
हैदराबाद का भारत में विलय
- 1947 में हैदराबाद के निजाम ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया
- हैदराबाद रियासत एक बहुत बड़ी रियासत थी जो चारों तरफ से भारत के इलाके से घिरी हुई थी।
- हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था
- हैदराबाद रियासत के लोगों ने निजाम केे शासन खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया साथ तेलंगाना खिलाफ इलाके के किसानो ने भी निजाम के शासन से दुखी होकर निजाम के खिलाफ आंदोलन किया।
- हैदराबाद शहर आंदोलन का गढ़ बन चुका था इसीलिए निजाम ने अपने अर्धसैनिक बल रजाकार को आंदोलन दबाने के लिए भेजा ।
- रजाकारों ने हैदराबाद रियासत में गैर मुसलमानो को निशाना बनाकर लुटपात, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया।
- इन सारी घटनाओं की सूचना प्राप्त होने के बाद 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना की मदद लेकर निजाम के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की इस कार्यवाही को देखकर निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया।
- इस तरह सैन्य कार्यवाही के आधार पर हैदराबाद रियासत का विलय भारत में किया गया।
मणिपुर रियासत का विलय
- मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोधचंद्र सिंह व भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए।
- जनता के दबाव में जून 1948 में निर्वाचन करवाया गया इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ।
- मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए।
- अंततः भारत सरकार, मणिपुर को भारतीय संघ में विलय कराने में सफल हुई।
राज्यों का पुनर्गठन
- औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतो का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की माँग हुई।
- भाषा के आधार पर प्रांतो के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन (1920) में पहली बार शामिल किया गया था।
- तेलगुभाषी, लोगों ने माँग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगुभाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए।
- आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोट्टी श्री रामुलू की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई।
- इसके कारण सरकार को दिसम्बर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार आंध्रप्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना।
- 1953 में केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया।
आयोग की प्रमुख सिफारिशे
1) त्रिस्तरीय (भाग A,B,C) राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए।
2) केवल 3 केन्द्रशासित क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मणिपुर) को छोड़कर बाकी के केन्द्रशासित क्षेत्रों को उनके नजदीकी राज्यों में मिला दिया जाए।
3) राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए।
इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और देश को 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों में बाँटा गया।
ncert Class 12 Political Science book 2 Chapter 1 Notes in Hindi
के notes आपको कैसे लगे अपनी राय जरूर दे